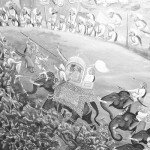ऋग्वेद अनुवाद मण्डल १ सूक्त १
- अग्नि अभीप्सा है मेरी, मेरा प्रतिनिधि, यज्ञ की दिव्यता और सत से आनंदित। वे आवाहन करते हैं और सभी प्रकार के आनंद धारण करते हैं।
- अग्नि जो प्राचीन ऋषियों को प्रिय थे नए ऋषियों की भी आकांक्षा हैं। वे अन्य देवों को संग लिए यहाँ आगमन करें।
- अग्नि के द्वारा प्राप्त होता है हमें वह ( आध्यात्मिक) ऐश्वर्य जो दिन- प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैभव और वीरता से पूर्ण।
- हे अग्नि! वह तीर्थ- यज्ञ जो सभी ओर से तुम समाहित करते हो, वह ही देवों तक पहुँचता है।
- अग्नि जो यज्ञ का आवाहन करते हैं, जिनकी दृष्टि जगत से परे है और जो परमात्मा की इच्छाशक्ति हैं, ज्वलंत प्रेरणाओं के अधिपति हैं। और सभी देव भी उनके साथ आगमन करें।
- हे अग्नि! वह आनंदमय शुभ जो तुम दाता के लिए उत्पन्न करते हो वही सत्य है और वह तुम्हारा ही सत्य है, हे अंगिरस!
- तुम्हारी ओर, हे अग्नि! हम दिन प्रतिदिन, रात्रि हो या प्रकाश, आते हैं, हमारे ध्यान में तुम्हारा लिए श्रद्धा वहन किए।
- तुम्हारे लिए, जो हमारे तीर्थ- यज्ञ पर राज्य करते हो, सत्य के आलोकित रक्षक, अपने गृह में वृद्धि करते हुए।
- इसलिए, हमारे लिए सरलता से उपलब्ध रहो जैसे पिता पुत्र के लिए, हमारी उल्लासमय अवस्था के लिए हमारे साथ संयुक्त रहो।
भावार्थ:
इस सूक्त से वैदिक योग का आरम्भ। आरम्भ आवाहन से व जागृति से। उस शक्ति का आभास करने का यत्न जो हमारी दिव्यता है, हमारे जीवन का केंद्र व संचालक है। जो हममें गुप्त या अचेतन इच्छाशक्ति है जो हमारे जाने अनजाने हमारी यात्रा प्रदर्शित करती है।
यह शक्ति और तेज जिसे हम अग्नि कहते हैं सत और चित्त से संचार का माध्यम है, हमारे दूत हैं जो हमें विश्व की सभी दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं। इनसे हमारा सम्बंध आत्मिक व अंतरंग है और हमारा योग इन्हें हममें प्रतिदिन सशक्त करने का प्रयास है। और बहुत कुछ किंतु संक्षेप में यह इसका सार।
(अनुवाद श्री अरविंद की टीका व भाष्य पर आधारित)
विवेचना: अग्नि वेद में प्रतीक हैं जिनसे अर्थ है तेज शक्ति के देव। अग्नि से अर्थ हमारी भीतरी दिव्यता। किंतु अग्नि के और भी अनेक भाव हैं। जैसे यज्ञ में हमारे पुरोहित या हमारा अग्र भाग हैं , हमारे प्रतिनिधि। जैसे वे आवाहन करने वाले होतार हैं और देवताओं के दूत हैं और ऋत्विज हैं अर्थात् जिन्हें सत्य से आनंद पहुँचता है।
यज्ञ से अर्थ बाहरी अग्नि जला कर उसमें घी उंडेल देवताओं से कुछ भौतिक भेंट प्राप्त करना नहीं, बल्कि यज्ञ से अर्थ हैं परमात्मा को आत्मसमर्पण। यज्ञ के पंद्रह अर्थ हैं जिनमें मुख्य हैं विष्णु, योग, धर्म, स्वयं का उत्सर्ग, आदि।
प्रथम ऋक् में अग्नि का वर्णन है व उनकी मुख्य विशेषताओं का चित्रण।
पुरोहित से अर्थ पंडित नहीं। पुरोहित शब्द आया है पुरत: से जिसका अर्थ है अग्रिम भाग। अर्थात् अग्नि जो हमारा पुरोहित है हमारा मुख है, हमारे वह अंग जो जगत का सामना करे और हमारे सभी अनुषठानों का नेतृत्व करे। वह इच्छाशक्ति जिसके पीछे हमारा जीवन चलता है वह अग्नि।
ऋग्वेद आध्यात्म का उच्चतम ग्रंथ है किंतु इसे समझने के लिए इसकी कुंजी समझनी होगी। वह सूत्र है इसके प्रतीक और श्लेष व यमक अलंकार जिनसे कई स्तरों पर अर्थ निकलते हैं। वेद अनूठा बहुआयामी साहित्य हैं जिनमें लय, अर्थ, संकेत व बिम्ब कम से कम तीन लोकों का वर्णन करते हैं: आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक।
ऋग्वेद दो शब्दों से बना है ऋक् व वेद। ऋक् से अर्थ प्रशंसा व वेद से अर्थ जानना या ज्ञान। ऋक् शब्द के मूल का अर्थ प्रकाश भी है और गीत भी।ऋग्वेद कम से कम ४००० साल पहले पृष्ठ पर उतारे गए किंतु इनकी पाठ, उच्चारण, संरचना व रीति उससे कई हज़ार वर्ष पुरानी है।
ऋग्वेद में लगभग १०, ००० मंत्र हैं। मंत्र से अर्थ काव्य की चरम सीमा जहां दर्शन, शैली, विचार व ध्वनि एक होकर भाव को अनुभूति में परिवर्तित कर देते हैं। मंत्र वह जो मन को एकाग्र कर मुक्त कर दे और उसका उच्चारण व श्रवण ही योगसाधना हो।
ऋग्वेद के अध्ययन के विभिन्न विषय छः हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। ये हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और छंद।
वैदिक छंद अत्यंत ही विकसित व परिमार्जित है। इस पर आज भी शोध की जा रही और शोधकार हर वर्ष नई खोज करते हैं। वेद किन्हें देवों को प्रसन्न करके उनसे कुछ पाने के कारण कांड नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतीकात्मक विवरण हैं।
पहले मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे वे सदा शुभ ही करते हैं। भद्रम शब्द से अर्थ है वे जो सदा मंगल ही करें।
इस सूक्त में दोनों भक्ति और ज्ञान योग का प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। किस प्रकार मन केंद्रित होकर ऊर्जा से भर जाता है और किस प्रकार ऋषि भक्ति भाव से भरकर अग्नि को नमन करते हैं।
अग्नि केवल ज्वाला नहीं। वे हमें पवित्र करते हैं। चाहे इनमें कुछ भी अशुद्ध वस्तु डाली जाए ये उसे पवित्र ही करते हैं। इसी शुद्धि से अस्तित्व का आनंद या सोम उठता है जो योग में अत्यंत सहायक है।
अग्नि जातवेदस हैं अर्थात् इन्हें हमारे जन्मों का ज्ञान है। इनका ओज आग ही नहीं आलोक भी है। अर्थात् अग्नि ज्वाला और प्रकाश दोनों हैं। अग्नि कई प्रकार की हैं, जैसे सौर्य अग्नि जो सूर्य का तत्व है, विद्युत अग्नि जो इंद्र या दिव्य मन का अस्त्र है। किंतु अग्नि जल में भी छिपी हुई है और वे अचेतन में भी गुप्त हैं। जैसे जैसे अग्नि शक्तिमान होती है योग व यज्ञ दोनो भी ऊर्जा व प्रभाव से भर जाते हैं।
अग्नि का गृह है सत्यम ऋतम बृहत्। वहीं उनका सही रूप देखा जाता है। किंतु फिर भी सभी देवों में मनुष्य के सबसे समीप अग्नि ही हैं।
और देव से अर्थ है दिव्य, दीप्तिमान, जो केवल देते हैं और द्यौस में रमण करते हैं। सभी देव एक ही परमात्मा की शक्तियाँ हैं और उन्हीं में उनकी पूर्णता है।
निरुक्त — अग्नि शब्द तीन मूल ध्वनियों से आया है। अ- बीज ध्वनि जो आरम्भ और अस्तित्व का भाव देती है। ग्- मूल से भाव है शक्ति का। अग्- से अर्थ है जो आगे हो, श्रेष्ठ और प्रख्यात, ज्वलंत, शक्तिमान, अप्रतिम। और अग्नि से अर्थ हुआ वह जो महान, उत्तम, बलवान, उद्दीप्त, और नेतृत्व करने के योग्य हो। अग्- मूल से ही आए है और शब्द जैसे आंग्ल भाषा में Agnes, igneous, ignite. निरुक्त के कारण कई शब्द द्वि- या त्रि- अर्थी होते हैं जिससे वेद के बहुस्तरीय व बहुआयामी अर्थ निकलते हैं।
व्याकरण: पहले पाँच मंत्रों का आरम्भ अग्नि की विभिन्न विभक्तियों से हुआ है। इससे स्मृति में भी सरलता होती है। अगले चार मंत्रों में से तीन में फिर अग्नि की विभक्तियाँ देखी जा सकती हैं किंतु मंत्र के आरम्भ में नहीं।
छंद: वेद में छंद अत्यंत विकसित व परिमार्जित है। पहले सूक्त में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है जिसमें तीन पद होते हैं, प्रत्येक में आठ वर्ण। अनुप्रास, यमक व श्लेष अलंकारों का प्रयोग खुल कर किया गया है किंतु हर बार अलंकार का प्रयोग विशेष कारण से किया जाता है। स्वामी दयानंद के अनुसार अग्नि स्वयं ही श्लेष है क्योंकि वह भौतिक भी है तो आध्यात्मिक शक्ति भी। यास्क मुनि के अनुसार वेद के तीन स्तरों पर अर्थ निकलते हैं जिसका मुख्य कारण संकेत या symbol का प्रयोग है। तुक या अंत्यानुप्रास भी देखा जाता किंतु वह कई बार आंतरिक या internal होता है। रूपक व उपमा का प्रयोग भी सहजता से उपयुक्त हुआ है।